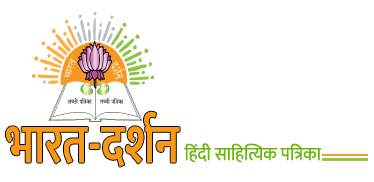मेरा पासपोर्ट कहीं खो गया था। मुझे याद है कि पिछली बार मैंने उसे अपने बैग में रखा था। अपनी चीज़ों के मामले में मैं बहुत लापरवाह हूँ। मैं बैग को अपने दफ़्तर के कमरे में रखकर उसे भूल जाता था और उसे तभी याद करता था, जब मुझे उसमें से कुछ चाहिए होता था या उसे उठाकर घर जाना होता था। मुझे लगता था कि किसी ने पासपोर्ट मेरे बैग से निकाल लिया था। निकालने वाला उसका क्या इस्तेमाल करना चाहता होगा, कह नहीं सकते। यों वह सरकारी पासपोर्ट था और कोई उसका कई तरह से दुरुपयोग कर सकता था।
पासपोर्ट के खोने के स्थान के बारे में इतना निश्चित होने के बावजूद मैंने उसे हर उस जगह तलाश करने की कोशिश की, जहाँ वह हो सकता था, बल्कि मैंने तो उसे वहाँ भी तलाश किया, जहाँ उसके होने की संभावना न के बराबर थी। पर उस कमबख़्त को नहीं मिलना था, सो नहीं मिला। जब मैं उसकी इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा था, तो पत्नी ने तलाश किए जाने वाली वस्तु के बारे में जानना चाहा। मैंने बता दिया। सोचा कि हो सकता है, उसी ने कहीं रख दिया हो या कहीं रखा हुआ देखा हो, लेकिन उसके पास तो इस सारी कवायद पर केवल यह टिप्पणी थी - “जाने किन खयालों में रहते हो, अपनी चीज़ें भी नहीं संभाल सकते।”
दरअसल, पासपोर्ट यों बैग में रखकर ले जाने वाली चीज़ नहीं है। दूतावास-कर्मियों को रूसी विदेश विभाग एक विशेष पहचान-पत्र जारी करता था, जिसे पास में रखना और ज़रूरत होने पर जाँच के लिए पेश कर देना न केवल काफ़ी था, बल्कि बहुत सम्मानजनक भी था। लेकिन मॉस्को में मिलित्सिया वालों (पुलिस वालों) ने इस चीज़ को हौवा जैसा बना रखा था। वे हम काले-पीले भारतीयों को देखते ही तुरंत हमारे पास आते, सलाम ठोंकते - ज़्द्रास्तवुते गास्पादि (महिला होने पर गास्पाज़ा), और कहते - दाक्यूमेंत पज़ालस्ता (कृपया दस्तावेज़ दिखाइए)। और नियम के हिसाब से उन्हें यह हक भी था।
मॉस्को में कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति नहीं रह सकता था, यह उस देश का नियम था। वहाँ अनेक लोग नाजाएज़ तरीके से रहते होंगे, जिन्हें पकड़ना उनका काम था। उन लोगों में ज़्यादातर लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आदि देशों के थे जो सब मिलकर भारतीयों जैसे ही दिखते थे और चूँकि रूस में भारतीयों की अभी भी काफ़ी इज्ज़त थी, इसलिए वे खुद को भारतीय ही कहते थे और इस ओढ़ी हुई पहचान का जो लाभ मिल सकता था, उसे उठाते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में वे भारतीयों की साख को वहाँ कम करते जा रहे थे, क्योंकि सब लोग सोचने लगते थे कि जो कुछ ग़लत काम हो रहे हैं, वे भारतीयों के कारण ही हो रहे हैं। और ये ग़लत काम काफ़ी थे, जैसे - बिना वीज़ा के रहना, रूसी लड़की को प्रेम-जाल में फँसाकर उसे गर्भ उपहार में देकर गायब हो जाना, मेट्रो स्टेशन पर छोटा-मोटा धंधा शुरू कर देना, हवाले का काम करना, बिना लाइसेंस के व्यापार करना, रिश्वत देकर काम निकलवाना, आदि।
खैर, मिलित्सिया वाले गाहे-बगाहे एशियाई लोगों से और अपने से अलग हुए देशों (जैसे बेलारूस) के लोगों से उनकी पहचान के दस्तावेज़ (पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि) माँगते थे। इतने तक तो ठीक था, लेकिन उनका उद्देश्य ग़लत लोगों को पकड़ना नहीं होता था, बल्कि बिना दस्तावेज़ के लोगों से कुछ पैसा ऐंठ लेना भर होता था। यदि व्यक्ति दस्तावेज़ निकालकर दिखा देता था, तो वे बहुत निराश होते और जब किसी के पास दस्तावेज नहीं होता था, तो उनकी प्रसन्नता वैसी ही होती, जैसी बंसी में मछली फँस जाने पर मछलीमार की होती है। वे उस व्यक्ति को एक ओर ले जाते और रूसी भाषा में गिटर-पिटर शुरू कर देते। अब अगर व्यक्ति को रूसी भाषा नहीं आती होती, तो स्थिति और बिगड़ जाती, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि मिलित्सिया वाले को कैसे समझाए कि वह कौन है और कैसे उसका दस्तावेज़ घर पर छूट गया है, आदि। शीघ्र ही मिलित्सिया वाले रूबल्या-रूबल्या का जाप शुरू कर देते और रूसी से अनभिज्ञ व्यक्ति भी समझ लेता कि कुछ रूबल देकर जान छुड़ाई जा सकती है। एक दो बार ऐसा होने के बाद व्यक्ति संभल जाता और उसे पता चल जाता कि ऐसी स्थिति में क्या करना है।
ऐसा भी नहीं था कि दस्तावेज़ दिखाने पर मिलित्सिया वाले छोड़ ही देते हों। वे शिकार को भाँपने की कोशिश करते थे। अगर उन्हें लगता था कि शिकार कमज़ोर है, तो वे दस्तावेज़ दिखाने वाले व्यक्ति से भी रूबल ऐंठ लेते थे। वे दस्तावेज़ को बहुत देर तक गौर से देखते रहते, उसकी तारीख़ पढ़ते रहते, फ़ोटो का व्यक्ति से मिलान करते रहते, और इस कोशिश में रहते कि कोई ग़लती मिल जाए, तो काम बने। कभी-कभी कोई बहादुर मिलित्सिया वाला तो ग़लती न मिलने पर भी अपना काम कर जाता था। श्रीमती राम के साथ यही हुआ था। वे अपनी सहेलियों के साथ बाज़ार गई थीं। मिलित्सिया वाले के माँगने पर उन्होंने तुरंत पहचान-पत्र दिखा दिया, क्योंकि इस बात का प्रशिक्षण हर भारतीय को अपने परिवार, सहकर्मियों, मित्रों वगैरह से रूस की ज़मीन पर पैर रखने से तुरंत ही मिल जाता था। लेकिन मिलित्सिया वाला रूसी में कुछ-कुछ बोलता रहा और तंग आकर उन्हें पचास रूबल देकर पिंड छुड़ाना पड़ा। इस बीच बाकी सहेलियाँ वहाँ किंकर्तव्यविमूढ़ और इस बात से प्रसन्न खड़ी रहीं कि चलो, हमारी जान तो बची।
ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए हम लोग घर से बाहर निकलने से पहले ठंड से बचने के लिए टोपी, मफ़लर, दस्ताने वगैरह के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर लेते थे कि जेब में पहचान-पत्र है। यहाँ तक कि कोई दूसरी चीज़ भले ही छूट जाए, पर पहचान-पत्र नहीं छोड़ते थे। लेकिन आदमी ही तो है, कभी भूल भी सकता है। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं पहचान-पत्र घर पर भूल गया और एक फर्लांग जाते ही मुझे मिलित्सिया वाला भी दिख गया। ऐसा भी होता था कि जब पहचान-पत्र वगैरह पास में होता था, तो मिलित्सिया वाला नहीं दिखता और जब नहीं होता, तो वह तुरंत प्रकट हो जाता है। तो उसे देखते ही मेरा हाथ जेब पर गया और वहाँ पहचान-पत्र नहीं था।
मैं तुरंत उलटे पैर लौट पड़ा। मैंने सोचा कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी होगी। मेरा इरादा था कि फुर्ती से जाकर पहचान-पत्र ले लूँ और इस मुसीबत से बचूँ। लेकिन मिलित्सिया वाला मुझे भाँप गया। पक्का खिलाड़ी था। इतने दिनों तक मॉस्को की सड़कों पर बर्फ़ थोड़े ही छानी थी। वह मेरे पीछे लपका और “ज़्द्रास्तवुते दाक्यूमेंत पज़ालस्ता” वगैरह कहता हुआ नज़दीक आने लगा। मैं जान चुका था कि वह मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन यह बात नज़रअंदाज़ करते हुए मैं अपनी गति से घर की ओर बढ़ता रहा।
वह भागकर बिल्कुल साथ आ गया और फिर “ज़्द्रास्तवुते दाक्यूमेंत पज़ालस्ता” का राग अलापने लगा। मैंने रूसी में कहा, अभी दिखाता हूँ और फिर घर की ओर चलता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इतने में घर आ गया।
मॉस्को में हर घर (वहाँ घर का मतलब अनेक फ़्लैट) में, ख़ास तौर से राजनयिक घरों में एक अखराना (चौकीदार) होता है। मुझे मिलित्सिया वाले के साथ देखकर हमारे घर का अखराना मदद के लिए आ गया। उनकी आपस में बात हुई। मैंने मिलित्सिया वाले को वहीं रुकने के लिए कहा, पर उसने कहा कि वह भी साथ चलेगा। मुझे उसके साथ अकेले लिफ़्ट में जाना निरापद नहीं लगा। खैर, मेरे कुछ कहने से पहले ही अखराना भी या तो मुझे परेशानी से बचाने के लिए या फिर अपने कर्तव्य के वशीभूत हमारे साथ हो लिया। मैंने राहत की साँस ली।
पत्नी ने दरवाज़ा खोला और मुझे इन रूसियों के साथ देखकर परेशान हो गई। मैंने जल्दी से उसे सारी बात बताई और घर में घुस गया और उसे कहा कि दरवाज़ा बंद कर ले। वह दरवाज़ा बंद करने लगी, तो उस मिलित्सिया वाले ने ज़ोर से ठोकर मारकर दरवाज़ा खोल दिया। इस बीच मैंने अपना पहचान-पत्र उठा लिया था और बाहर आकर उसे मिलित्सिया वाले के सामने पेश कर दिया। वह संतुष्ट हो गया और “अगर सड़क पर ही इसे दिखा देते, तो इतनी परेशानी न होती” कहता हुआ चला गया।
मैंने फिर राहत की साँस ली, इस बार ज़रा लंबी ही, लेकिन एक डर मन में बैठ गया कि अगर अगली बार ऐसा होगा और अगर घर से दूर होगा, तो बड़ी ले-दे होगी। और तब से पहचान-पत्र के अलावा मैं अपने बैग में पासपोर्ट भी रखने लगा, ताकि यदि ग़लती से पहचान-पत्र छूट भी जाए, तो पासपोर्ट दिखाकर जान बचाई जा सके। आप पूछ सकते हैं कि यदि दोनों ही घर पर छूट जाएँ, तो मैं क्या करूँगा? तब मैं आपसे पूछूँगा कि आप मेरे साथ हैं या मिलित्सिया वाले के साथ?
इसी अति-सावधानी के चलते पासपोर्ट कहीं खो गया था।
मैंने दूतावास को इस गुमशुदगी की सूचना दे दी और नया पासपोर्ट बनाने की अर्जी भी दे दी। सामान्यतः पासपोर्ट की अनुलिपि बिना किसी विशेष औपचारिकता के बना दी जाती थी, लेकिन क्योंकि विदेश विभाग के कर्मचारी हम अध्यापकों को बाहरी व्यक्ति मानते थे और काफ़ी हद तक हमारे अधिक वेतन, कम काम, और विशेष रूप से हमारी कक्षाओं में आने वाली सुंदर रूसी कन्याओं के कारण हमसे द्वेष-भाव रखते थे, इसलिए एक क्लर्क ने टिप्पणी लिखकर भेज दी कि नियमानुसार एफ़.आई.आर. के बाद ही नया पासपोर्ट जारी हो सकता है।
इसके बाद एफ़.आई.आर. की कवायद शुरू हुई। कार्यालय की दुभाषिया नताशा के साथ मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा। वह वहाँ के अधिकारी के साथ काफ़ी देर तक बात करती रही, उसे सारा मामला समझाया, उसके सवालों के जवाब दिए कि पासपोर्ट कहाँ खोया, क्यों खोया, कब खोया, आदि और एफ़.आई.आर. दर्ज करने के लिए कहा। तब उस अधिकारी ने जानकारी दी कि एफ़.आई.आर. तो फलाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज होती हैं। और इस तरह हम वहाँ से बैरंग लौट आए। मैं अलबत्ता सोचता रहा कि अगर यहाँ एफ़.आई.आर. दर्ज नहीं हो सकती थी, तो उसने इतनी पूछताछ क्यों की?
अगले दिन हम फलाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे और वही सिलसिला वहाँ भी दोहराया गया। पूरी पूछताछ के बाद अंत में वहाँ के अधिकारी ने बताया कि राजनयिक एफ़.आई.आर. तो “क” पुलिस स्टेशन में दर्ज होती हैं। हम फिर लौट आए।
दो दिन बाद “क” पुलिस स्टेशन पहुँचे। मैंने दुभाषिये को कहा कि इस बार वह पहले ही पूछ ले कि यहाँ एफ़.आई.आर. हो भी सकती है या नहीं। उसने पूछ लिया और वहाँ से उत्तर सकारात्मक मिला। फिर वही पूछताछ का सिलसिला चला। अंत में वहाँ के अधिकारी ने बताया कि जहाँ पासपोर्ट खोया है, वह इलाका “ख” पुलिस स्टेशन के कार्यक्षेत्र में आता है और इस तरह हमारी चुस्ती काम नहीं आई और हमें फिर लौटना पड़ा।
“श्रीमान विकास, क्या आपको मालूम है कि “ख” पुलिस स्टेशन कौन-सा है?” बाहर आकर दुभाषिये ने मुझसे पूछा।
“नहीं।” मुझे नहीं मालूम था।
“वही, जिसमें हम सबसे पहले गए थे।” उस रूसी दुभाषिये ने झल्लाते हुए कहा, “मूर्ख रूसी, पता नहीं ये लोग हमें यहाँ से वहाँ क्यों धकिया रहे हैं!”
हम कार्यालय में लौट आए। वहाँ हमारा संदेशवाहक गिनाडी मिला। वह हँसमुख और बातूनी व्यक्ति था। मुझे और नताशा को परेशान देखकर उसने पूछा, “गास्पादिन विकास, क्या परेशानी है?”
“तुम्हारी समझ में नहीं आएगा!” नताशा ने उसे दुत्कार दिया। उसे लगा होगा कि जिस काम को वह योग्य होने के बावजूद इतना समय और ऊर्जा लगाकर भी नहीं कर पा रही, वह काम कम पढ़ा-लिखा और अंग्रेज़ी न जानने वाला गिनाडी भला कैसे कर सकता है!
गिनाडी ने नताशा की टिप्पणी पर गौर नहीं किया और आँखों-ही-आँखों में मुझसे पूछा। मुझे लगा कि उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है और वैसे भी हम बहुत-सी बातें उससे बाँटते ही थे। नताशा के न चाहते हुए भी मैंने उसे सब बता दिया।
“काकिई प्रोब्लैम!” गिनाडी ने हँसकर कहा, “यह काम तो एक दिन में हो सकता है और श्रीमान विकास को वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है।” गिनाडी ने नताशा से कहा।
नताशा चुप रही, लेकिन मैं बार-बार धक्के खाने और काम न होने की हताशा के बाद इतना दुखी हो चुका था कि तुरंत उत्सुकता-से बोला, “वो कैसे?”
“बस एक स्मिरनोफ़ की बोतल चाहिए।” गिनाडी ने अपने दाँत दिखाते हुए और टोपी उतारते हुए कहा। उसकी छोटी-छोटी बिल्लौरी आँखें भी हँस रही थीं।
सौदा तय हो गया। मैंने अगले ही दिन उसे स्मिरनोफ़ की दो बोतलें लाकर दे दीं – एक जो उसने माँगी थी और दूसरी उसके लिए। वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अपने लिए वोदका की उम्मीद नहीं थी।
स्मिरनोफ़ लेकर गिनाडी चला गया और दो घंटे बाद ही एफ़.आई.आर. की प्रतिलिपि लेकर आ गया।
-प्रो. राजेश कुमार